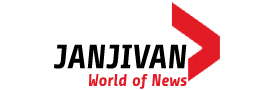मृत्युंजय कुमार
हाल में सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा 2019-20 के लिए राष्ट्रीय आय का अग्रिम अनुमान ( 5 प्रतिशत) जारी किया गया। दो तिमाहियों के खराब प्रदर्शन के बाद आये इस अनुमान से स्पष्ट है कि निकट भविष्ट में आर्थिक सुधार की तस्वीर साफ नहीं है। दिसंबर में 7.35 प्रतिशत पर पहुंची खुदरा महंगाई की चुनौती अलग से है। खाद्य पदार्थों के बढ़े दामों का दबाव शहर और गांव दोनों तरफ महसूस किया जा रहा है। आम बजट से पहले आये महंगाई के आंकड़ों, घटती मांग, रोजगार की कमी और विभिन्न समस्याओं से घिरी अर्थव्यवस्था के सुधार पर सरकार का रुख अहम होगा।
महंगाई एक बार फिर डरावने तरीके से दस्तक दे रही है। बीते दिसंबर में खुदरा महंगाई दर रिकॉर्ड 7.35 प्रतिशत पर पहुंच गयी। हालिया राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई दर दिसंबर, 2018 में 2.11 प्रतिशत थी, जो नवंबर, 2019 में 5.54 प्रतिशत पर पहुंच गयी थी।
इससे पहले जुलाई, 2014 में महंगाई दर 7.39 प्रतिशत पर पहुंची थी। दिसंबर, 2018 के मुकाबले बीते महीने सब्जियों की कीमतों में 60.5 प्रतिशत की महंगाई दर्ज की गई। प्याज की पैदावार में 26 प्रतिशत की गिरावट की वजह से देश के कई प्रमुख शहरों में प्याज की कीमतें 150 रुपये से अधिक हो गयी थीं।
कुल मिलाकर दिसंबर महीने में खाद्य महंगाई बढ़कर 14.12 प्रतिशत रही, जो बीते वर्ष इसी अवधि में -2.65 प्रतिशत दर्ज की गयी थी। नवंबर, 2019 में यह आंकड़ा 10.01 प्रतिशत पर था, जिसमें तेजी से उछाल आया है। सब्जियों के अलावा दालों, मीट, मछली की कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दालों में जहां 15.44 प्रतिशत, वहीं मीट और मछली की कीमतों में लगभग 10 प्रतिशत की तेजी आयी है।
सिरदर्द बनेगी महंगाई !
नवंबर, 2019 के मुकाबले दिसंबर, 2019 में 1.81 प्रतिशत की वृद्धि के साथ महंगाई दर 7.35 प्रतिशत पर पहुंच गयी। आरबीआइ द्वारा निर्धारित महंगाई की 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा पार करने से विभिन्न स्तरों पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। अगर खाद्य कीमतें नियंत्रित नहीं होती हैं, तो यह समस्या और बड़ी हो सकती है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात की आशंका थी, इसलिए ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया था।
आरबीआइ द्वारा जारी बयान में 2019-20 की दूसरी छमाही में महंगाई दर 4.7 से 5.1 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान था, लेकिन यह भी कहा गया था कि खाद्य कीमतों में राहत होने से यह खुदरा महंगाई 2020-21 की पहली छमाही में आरामदेह स्थिति यानी 3.8 से 4 प्रतिशत के बीच आ सकती है।
साल 2016 में आगामी पांच वर्ष के लिए सरकार द्वारा तय की गयी महंगाई की 2 से 6 प्रतिशत की प्रतिबद्धता सीमा पार होने से अब आरबीआइ के लिए चिंताजनक स्थिति है। महंगाई की चिंता के मद्देनजर दिसंबर की पॉलिसी में आरबीआइ ने रेपो दरों में बदलाव नहीं किया था, लेकिन आगामी 6 फरवरी की मासिक मौद्रिक नीति की घोषणा में आरबीआइ का क्या रुख होता है। यह देखना अहम होगा।
आरबीआइ का उदारवादी रवैया
महंगाई के छह साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से आरबीआइ द्वारा ब्याज दरों में आगे कटौती की संभावना कम है। अपनी पिछली नीतिगत समीक्षा में आरबीआइ ने उदारवादी रुख अपनाया था। हालांकि, बढ़ी ब्याज दरें न तो अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए और न ही मांग की कमी से जूझते बाजार के लिए अच्छी हैं, विशेषकर ऐसे वक्त में जब चार दशक में बेरोजगारी दर अधिकतम हो।
आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास कह चुके हैं कि सरकार के पास ही अब विकल्प बचे हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि महंगाई का मुद्दा मौद्रिक नीति समिति के आगे के निर्णयों को प्रभावित करेगा। आम बजट के पांच दिन बाद ही आरबीआइ अपनी नीतिगत समीक्षा करेगा, ऐसे में तैयार की गयी राजकोषीय योजनाओं पर महंगाई का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।
‘मूल स्फीति’ नहीं है चिंताजनक
बीते कुछ महीनों में तेजी से बढ़ी खुदरा महंगाई समस्याजनक है, लेकिन मूल स्फीति यानी कोर इनफ्लेशन की स्थिति अभी खराब नहीं है। मूल स्फीति में महंगाई सूचकांक तैयार करते समय अस्थिर कीमतों वाली वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। इसमें विशेषकर खाद्य और ईंधन शामिल होते हैं।
दिसंबर में भले ही खुदरा महंगाई में तेज उछाल आया है, लेकिन कोर इनफ्लेशन स्थिर है, इसकी वजह है कि मांग में कमी अभी बरकरार है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सब्जियों की कीमतों में गिरावट आने के बाद खुदरा महंगाई आरबीआइ की तय सीमा में आ सकती है।
एक उम्मीद है कि कृषि उत्पादों के दाम बढ़ने से ग्रामीण आय में वृद्धि हो सकती है, जो आर्थिक सुधार के नजरिये से आवश्यक भी है। लेकिन, लंबी अवधि तक खाद्य कीमतों के बढ़ने से आमजन के घर का बजट बिगड़ सकता है और अन्य मांगों में कटौती हो सकती है। जब कुल मिलाकर मांग में गिरावट की स्थिति है, ऐसे में मौजूदा महंगाई और चिंताजनक हो सकती है।
खुदरा महंगाई के बावजूद सेंसेक्स में उछाल
बीते दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई के पांच साल के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बावजूद सेंसेक्स में उछाल जारी है। सीपीआइ के अलावा बीते हफ्ते जारी थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) दिसंबर में 2.59 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो नवंबर में 0.58 प्रतिशत पर था।
सेंसेक्स इस हफ्ते 41,952.63 और निफ्टी 12,362.30 पर पहुंचा था। विशेषज्ञों का मानना है कि सीपीआइ में अचानक आये बदलाव के बावजूद बाजार बजट और तीसरी तिमाही में लाभ अर्जन के आशावादी नजरिये से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव के कम होने की उम्मीद है, इससे विश्व बाजार में सकारात्मक संकेत उभर रहे हैं।
उपभोक्ता मूल्य महंगाई : सामान्य बनाम खाद्य
कितनी गुंजाइश वर्तमान में भारत के समक्ष गिरती मांग और बढ़ती महंगाई की दोहरी चुनौती है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, यह ‘मुद्रास्फीति जनित मंदी’ (स्टेगफ्लेशन) की स्थिति है। बेरोजगारी की समस्या एक अलग ही चुनौती है। बजट से पहले मांग नहीं होने के बावजूद बढ़ती महंगाई सरकार के लिए चिंताजनक है।
आरबीआई के पास सीमित विकल्पों की वजह से आगे सरकार का रुख अहम होगा। कृषि क्षेत्र पर सरकार को फोकस करने की जरूरत है। रबी फसलों के उत्पादन के बाद ही स्थिति साफ हो पायेगी। अपेक्षित राजस्व संग्रह में आयी कमी की वजह से आनेवाले बजट में सरकार के पास सीमित विकल्प होंगे।
कॉरपोरेट दरों में कटौती और बढ़ी तेल कीमतों की वजह से भी समस्या उत्पन्न हुई है। नोबेल विजेता अभिजीत मुखर्जी समेत कई आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ठोस आर्थिक सुधार के लिए सरकार को कुछ समय के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य के इतर विकास पर फोकस करना चाहिए।
सरकार के लिए चुनौती
मौजूदा बढ़ी महंगाई के अलावा 2019-20 में 5 प्रतिशत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर सरकार और वित्त मंत्रालय के सुधार प्रयासों में बाधक बन सकती है। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि बजट का फोकस ‘आमजन’ पर होगा। जबकि, विशेषज्ञों का कहना है कि श्रम आधारित क्षेत्रों- विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन और रीयल एस्टेट आदि में सरकार को खर्च बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।
प्याज कीमतों में गिरावट के बावजूद सरकार को महंगाई के उतार-चढ़ाव पर बारीक नजर रखनी होगी। कुछ विशेषज्ञों का साफ कहना है कि सरकार को कम से कम मॉनसून तक सरकारी खर्च द्वारा विकास दर को बढ़ाना होगा। सितंबर के बाद महंगाई के नियंत्रित होने का अनुमान लगाया जा रहा है.
खाद्य महंगाई कितनी गंभीर
उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) मुद्रास्फीति में अचानक से हुई वृद्धि ने सभी को चौंकाया है। अगर इसे सितंबर 2016 से अगस्त 2019 की विस्तारित अवधि के लिए देखें, तो वर्ष-दर-वर्ष खाद्य कीमतों की वृद्धि (सीएफपीआइ इन्फ्लेशन) लगातार समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (सीपीआइ इन्फ्लेशन) से नीचे बनी रही। लेकिन यह वृद्धि अगस्त में 2.99 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 5.11 प्रतिशत, अक्तूबर में 7.88 प्रतिशत, नवंबर में 10.1 प्रतिशत और दिसंबर में 14.12 प्रतिशत पर पहुंच गयी।
प्याज की कीमतों में इजाफा
बीते महीने खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि मार्च के बाद से प्याज की कीमतों में 400 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार, अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन से प्याज की महंगाई को निकाल दिया जाये, तो खुदरा महंगाई दर 4.48 प्रतिशत पर आ जायेगी।
वर्ष 2008 से 2018 के बीच डॉलर की तुलना में रुपये का मूल्य 42 से 68 हो गया था, जो अब 70 के ऊपर है। लेकिन इस अवधि में शेयर बाजार सूचकांक दोगुने से भी अधिक है। अर्थव्यवस्था में लगातार कमी के बावजूद शेयर बाजार में बढ़त क्यों हो रही है। बाजार के जानकार आम तौर पर सलाह देते हैं कि निवेश के लिए सबसे अनुकूल समय तब होता है, जब सकल घरेलू उत्पादन की दर कम होती है।
लेकिन भारतीय शेयर बाजार मौजूदा स्तर पर समकक्ष बाजारों की तुलना में खर्चीला है। इस वजह से निवेश एक जोखिमभरा कदम भी है। इससे यह इंगित होता है कि अर्थव्यवस्था का सबसे खराब दौर बीत चुका है और आगे के लिए बहुत उम्मीदें हैं।
ये उम्मीदें बड़े निवेश के रूप में दिखायी दे रही हैं, भले ही उनके लिए कोई जमीनी आधार नहीं हो। उम्मीद का एक बड़ा कारण अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार द्वारा लगातार उठाये जा रहे कदम भी हैं। शेयर बाजार की उम्मीदों की बड़ी परीक्षा बजट की घोषणाओं के समय होगी। उद्योग जगत और निवेशकों को बड़े सुधारों की अपेक्षा है।
बेमौसम बारिश से मुश्किलें
अचानक से खाने की वस्तुओं के दाम आसमान छूने का एक प्रमुख कारण बेमौसम बारिश है। बीते वर्ष दक्षिण-पश्चिम मॉनसून (जून-सितंबर) में जुलाई के आखिरी हफ्ते तक काफी कम बारिश हुई। मॉनसून के देर से आने की वजह से खरीफ फसलों की बुवाई में देरी हुई। हालांकि, सितंबर, अक्तूबर, और यहां तक कि नवंबर में जमकर बारिश हुई, जिससे लगभग पक चुकी या कटाई के लिए खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। अत्यधिक या कम बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुए, जिससे सितंबर से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने लगीं।
रबी की बंपर पैदावार की उम्मीद
बेमौसम बारिश ने खरीफ की फसलों पर कहर बरपाया, हालांकि, उससे भूजल के स्तर बढ़ाने में मदद मिली। यह रबी की फसल के लिए लाभदायक है। किसानों ने चालू रबी मौसम में आठ प्रतिशत अधिक क्षेत्र में बुवाई की है। उम्मीद है कि इस बार बंफर फसल होगी।
कृषि मंत्रालय ने 2019-20 में खरीफ/ देर-खरीफ फसलों के कुल उत्पादन का अनुमान 54.73 लाख टन लगाया है, जो बीते वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत कम है। हालांकि, रबी की फसल मार्च अंत तक बाजार में आ जायेगी, इससे खाद्य पदार्थों की कीमतों के कम होने की उम्मीद है। यही बात कई अन्य सब्जियों पर भी लागू होगी।
उत्पादक और उपभोक्ता के हितों को संतुलित करे सरकार
खाद्य मुद्रास्फीति उन किसानों के लिए बुरी खबर नहीं है, जो फसल की कम कीमत मिलने और 2014 के बाद वैश्विक कमोडिटी बूम की समाप्ति से मुश्किल में हैं। खाद्य पदर्थों के मंहगे होने से उनका घाटा कम होगा और ग्रामीण आय में वृद्धि होगी, जो खपत और समग्र आर्थिक विकास के लिए फायदेमंद है़।
लेकिन सरकार और आरबीआइ खाद्य महंगाई को अनदेखा नहीं कर सकते। सरकार पर दाल, मिल्क पाउडर और खाद्य तेल जैसे खाने की वस्तुओं के अधिक आयात की अनुमति देने का दबाव है़ ऐसे में सरकार को उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों को संतुलित करने वाला निर्णय लेना होगा़।
खाद्यान्न भंडार संभालने की चुनौती
एक तरफ जहां खाद्य महंगाई छह साल के उच्चतम स्तर पर रही, वहीं दूसरी ओर सरकार के सामने चुनौती है कि वह खाद्यान्न के अब तक के उच्च स्तर के भंडार का प्रबंधन कैसे करे़। एक जनवरी, 2020 तक खाद्यान्न भंडार 75.51 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है़।
इस रबी सीजन में 330.20 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई हुई है, जो पिछले साल की तुलना में 33.23 लाख हेक्टेयर और 1950-51 के बाद से अब तक की सबसे अधिक बुवाई हुई है, इससे पहले वित्त वर्ष 2015 के दौरान 314.70 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं बोया गया था़।
इस दिसंबर 17 प्रतिशत से अधिक रहा एफएओ का बेंचमार्क सूचकांक
मार्च के बाद खाद्य कीमतों में कमी आएगी या नहीं, इसके लिए हमें वैश्विक मूल्यों पर ध्यान देना होगा़ 2000 का दशक कृषि उत्पादों के महंगे होने का दशक था़ वर्ष 2003 से 2011 के बीच संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन (एफएओ) का विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष : 2002-04 ) 97.7 के वार्षिक औसत से बढ़कर 229.9 पर पहुंच गया़।
लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट आयी और 2016 तक यह 161.5 पर आ गया़। लेकिन भारत में खाद्य कीमतों में आयी इस गिरावट में अब उलटफेर के संकेत दिख रहे हैं। दिसंबर 2019 में एफएओ का बेंचमार्क सूचकांक दिसंबर 2018 से 12.5 प्रतिशत अधिक था़। बेंचमार्क सूचकांक का अधिक होना अलग-अलग खाद्य पदार्थों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में सख्त प्रवृत्ति का संकेत हैं।